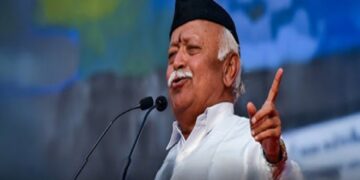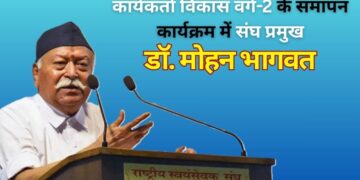पूरे भारत में जल्द ही जातिगत जनगणना होने जा रही है. इसका असर सभी राज्यों पर होने वाला है, उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं होगा. हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना के फैसले पर मुहर लगा दी है. इसका अर्थ ये है कि इस बार होने वाली गणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जातियों को भी शामिल किया जाएगा.
बता दें कि हमारे संविधान में अभी तक केवल एससी और एसटी की गणना करने का ही प्रावधान है, मगर इस बार ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाएगा. जातिगत जनगणना से उत्तराखंड में कई सामाजिक समीकरणों में बदलाव आने की संभावना है. आज इस आर्टिकल में प्रदेश के परिपेक्ष्य में जातियों के ताने-बाने को समझ कर इस कदम से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं.
उत्तराखंड की कुल जनसंख्या सवा करोड़ (1.22 करोड़) है. अनुमानित आंकड़ों की मानें तो उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, तो वहीं हरिद्वार लगभग 56 प्रतिशत, उधम सिंह नगर में 45 प्रतिशत तक इस वर्ग की हिस्सेदारी मानी जाती है.
उत्तराखंड की जनसंख्या: लगभग सवा करोड़. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार (1,00,86,292 करोड़) है.
जाति जनसंख्या आंकड़े
अनुसूचित जाति: 19%.
अनुसूचित जनजाति: 03%.
OBC और सामान्य वर्ग (GEN): 78%.
पूरे देश में साल 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है जिसके चलते ऊपर बताए गए आंकड़े उसी के आधार पर बताए गए हैं. उत्तराखंड में मुख्य रूप से सवर्ण, दलित, ओबीसी जैसी कई जातियां निवास करती हैं. हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में ओबीसी वर्ग बड़ी संख्या में निवास करता है. इसके अलावा मुख्य रूप से भोटिया, थारू, बरनौत, राजी, जौनसीरी, बुक्सा, जाड़ तथा दून के खड़वाल आदि जानजातियां पाई जाती हैं. ये सभी गढ़वाल हिमालय में पाई जाती है.
क्या है जातिगत जनगणना ?
बता दें कि जाति जनगणना शब्द तीन शब्दों (जाति+ जन+ गणना) से मिलकर बना है. जन का अर्थ होता है लोग और गणना का अर्थ होता है गिनती करना. इसका मतलब है कि जब लोगों से उनकी जाति पूछकर उनकी गिनती की जाती है. इसे करने का उद्देश्य ये पता लगाना है कि देश और स्थान विशेष में किस जाति के कितने लोग निवास करते हैं. जातिगत जनगणना से देश में निवास करने वाले SC/ST और OBC लोगों की जानकारी तो इकट्ठा होगी ही, इसके साथ ही उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का पता चलेगा.
जातिगत जनगणना के इतिहास और इसकी जरूरत
देश में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश काल में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी. हालांकि ये एक शुरुआती प्रयोग था, जिसे पूर्ण जनगणना नहीं माना जाता. इसके बाद पहली पूर्ण जनगणना साल 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पर की गई थी. इसमें पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी जारी किया गया था. इसके बाद से 10 साल के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती है.
साल 1881-1931 तक जातिगत जनगणना करवाई गई. इसके बाद इसे स्वतंत्र हुए भारत में बंद कर दिया गया. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में साल 2011 की जनगणना में जातिगत जनगणना हुई थी मगर इसके आंकडे़ ऑफिशियली जारी नहीं किए गए थे.
संविधान में जनगणना को लेकर क्या हैं प्रावधान?
भारतीय संविधान में जनगणना कराने को लेकर डीटेल में उल्लेख किया गया है. बता दें कि संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत जनगणना संघ सूचि का विषय है. यह संविधान की सातवीं अनुसूची के 69 नंबर में सूचीबद्ध है. यानि जनगणना कराने और उससे संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है. जबकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है. इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूचि में जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं.
जातिगत जनगणना के उत्तराखंड पर संभावित प्रभाव
- उत्तराखंड में जातिगत जनगणना करने से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनका सशक्तिकरण करने में मदद मिल सकती है. राज्य में 90 प्रतिशत जनजातियां ऐसी है जिन्हें पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिला हुआ है, मगर केवल ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत है. इससे ओबीसी वर्ग को दोबारा संगठित करने में मदद मिलेगी.
- उत्तराखंड में मूल रूप से पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू आदि हैं, इनकी जनसंख्या कुल आबादी का 2.89 प्रतिशत है. इन्हें मूल जनजातियों को ज्यादातर समय पर प्रदेश में अनदेखा किया गया है और इन्हें अपने मूलभूत अधिकारों के लिए भी आवाज उठानी पड़ी है. जातिगत जनगणना होने से इनकी पहचान हो सकेगी और इनके मुद्दों पर भी बात की जा सकेगी.
- उत्तराखंड भी प्रमुख समस्याओं में से एक पहाड़ों से होने वाला पलायन भी है, हर साल बड़ी संख्या में नौजवान लोग रोजगार की तलाश में अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं. इससे जहां एक तरफ जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, तो वहीं सुविधाओं पर दबाव भी पड़ रहा है. जातिगत जनगणना करने से इसे रोकने और युवाओं के लिए नई रोजगार संबंधी नीतियां बनाने में भी मदद मिल सकती हैं.